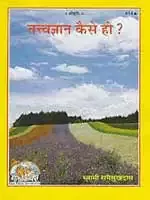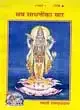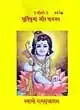|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> तत्वज्ञान कैसे हो तत्वज्ञान कैसे होस्वामी रामसुखदास
|
16 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है तत्त्वज्ञान कैसे हो...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
।।श्रीहरिः।।
नम्र निवेदन
प्रायः प्रत्येक साधक के भीतर यह जिज्ञासा रहती है कि तत्त्वज्ञान क्या है
? तत्त्वज्ञान सुगमता से कैसे हो सकता है ? आदि। इस जिज्ञासाकी पूर्ति
करने के लिये प्रस्तुत पुस्तक साधकों के लिये बड़े कामकी है। इसमें जो
बातें आयी हैं, वे केवल सीखने-सिखाने की, सुनने-सुनाने की नहीं हैं,
प्रत्युत अनुभव करने की हैं।
इस पुस्तक को पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तत्त्वज्ञान दूर से देखने में तो कठिन दीखता है, पर प्रवेश करने पर बड़ा ही सुगम और रसीला है।
परमात्मतत्त्व की खोज में लगे हुए साधकों से प्रार्थना है कि वे इस पुस्तक का अध्ययन-मनन करें और तत्त्व का अनुभव करें।
इस पुस्तक को पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तत्त्वज्ञान दूर से देखने में तो कठिन दीखता है, पर प्रवेश करने पर बड़ा ही सुगम और रसीला है।
परमात्मतत्त्व की खोज में लगे हुए साधकों से प्रार्थना है कि वे इस पुस्तक का अध्ययन-मनन करें और तत्त्व का अनुभव करें।
-प्रकाशक
1.तत्त्वज्ञान का सहज उपाय
हमारा स्वरूप चिन्मय सत्तामात्र है और उसमें अहम् नहीं है—यह
बात
यदि समझ में आ जाय तो इसी क्षण जीवनमुक्ति है ! इसमें समय लगने की बात
नहीं है। समय तो उसमें लगता है, जो अभी नहीं और जिसका निर्माण करना है। जो
अभी है, उसका निर्माण नहीं करना है, प्रत्युत उसकी तरफ दृष्टि डालनी है,
उसको स्वीकार करना है जैसे—
संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा।।
(मानस, बाल. 58/4)
दो अक्षर हैं—‘मैं हूँ’। इसमें
‘मैं’
प्रकृति का अंश है और ‘हूँ’ परमात्मा का अंश है।
‘मैं’ जड़ है और ‘हूँ’ चेतन है।
‘मैं’ आधेय है और ‘हूँ’ आधार है।
‘मैं’ प्रकाश्य है और ‘हूँ’
प्रकाशक है।
‘मैं’ परिवर्तनशील है और ‘हूँ’
अपरिवर्तनशील है।
‘मैं’ अनित्य है और ‘हूँ’ नित्य
है।
‘मैं’ विकारी है और ‘हूँ’
निर्विकार है।
‘मैं’ और ‘हूँ’ को मिला
लिया—यही
चिज्जडग्रन्थि (जड़-चेतन की ग्रन्थि) है, यही बन्धन है, यही अज्ञान है।
‘मैं’ और ‘हूँ’ को अलग-अलग अनुभव
करना ही मुक्ति
है तत्त्वबोध है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि
‘मैं’ को साथ
मिलाने से ही ‘हूँ’ कहा जाता है। अगर
‘मैं’ को
साथ न मिलायें तो ‘हूँ’ नहीं रहेगा, प्रत्युत
‘है’ रहेगा। वह ‘है’ ही अपना
स्वरूप है।
एक ही व्यक्ति अपने बापके सामने कहता है कि ‘मैं बेटा हूँ’, बेटे के सामने कहता है कि ‘मैं बाप हूँ’, दादा के सामने कहता है कि ‘मैं पोता हूँ’, पोता के सामने कहता है कि ‘मैं दादा हूँ’, बहन के सामने कहता है कि ‘मैं भाई हूँ’, पत्नी से के सामने कहता है कि ‘मैं पति हूं’, भानजे के सामने कहता है कि ‘मैं मामा हूँ’, मामा के सामने कहता है कि ‘मैं भानजा हूँ’ आदि-आदि। तात्पर्य है कि बेटा, बाप, पोता, दादा, भाई, पति, मामा, भानजा आदि तो अलग-अलग हैं, पर ‘हूँ’ सबमें एक है। ‘मैं’ तो बदला है, पर ‘हूँ’ नहीं बदला। वह ‘मैं’ बाप के सामने बेटा हो जाता, बेटे के सामने बाप हो जाता है अर्थात् वह जिसके सामने जाता है, वैसा ही हो जाता है। अगर उससे पूछें कि ‘तू कौन है’ तो उसको खुद का पता नहीं है ! यदि ‘मैं’ की खोज करें तो ‘मैं’ मिलेगा ही नहीं, प्रत्युत सत्ता मिलेगी। कारण कि वास्तव में सत्ता ‘है’ की ही है, ‘मैं’ की सत्ता है ही नहीं।
बेटे की अपेक्षा बाप है, बापकी अपेक्षा बेटा है—इस प्रकार बेटा, बाप, पोता, दादा आदि नाम अपेक्षासे (सापेक्ष) हैं; अतः ये स्वयं के नाम नहीं हैं। स्वयं का नाम तो निरपेक्ष ‘है’ है। वह ‘है’ ‘मैं’ को जाननेवाला है। ‘मैं’ जाननेवाला नहीं है और जो जाननेवाला है, वह ‘मैं’ नहीं है। ‘मैं’ ज्ञेय (जानने में आनेवाला) है और ‘है’ ज्ञाता (जाननेवाला) है। ‘मैं’ एकदेशीय है और उसको जानने वाला ‘है’ सर्वदेशीय है। ‘मैं’ से सम्बन्ध मानें या न मानें, ‘मैं’ की सत्ता नहीं है। सत्ता ‘है’ की ही है। परिवर्तन ‘मैं’ में होता है, ‘है’ में नहीं। ‘हूँ’ भी वास्तव में ‘है’ का ही अंश है। ‘मैं’ पनको पकड़ने से ही वह अंश है। अगर मैं-पन को न पकड़ें तो वह अंश (‘हूँ’) नहीं है, प्रत्युत ‘है’ (सत्ता मात्र है) ‘मैं’ अहंता और ‘मेरा बाप, मेरा बेटा’ आदि ममता है। अहंता-ममतासे रहित होते ही मुक्ति है—
एक ही व्यक्ति अपने बापके सामने कहता है कि ‘मैं बेटा हूँ’, बेटे के सामने कहता है कि ‘मैं बाप हूँ’, दादा के सामने कहता है कि ‘मैं पोता हूँ’, पोता के सामने कहता है कि ‘मैं दादा हूँ’, बहन के सामने कहता है कि ‘मैं भाई हूँ’, पत्नी से के सामने कहता है कि ‘मैं पति हूं’, भानजे के सामने कहता है कि ‘मैं मामा हूँ’, मामा के सामने कहता है कि ‘मैं भानजा हूँ’ आदि-आदि। तात्पर्य है कि बेटा, बाप, पोता, दादा, भाई, पति, मामा, भानजा आदि तो अलग-अलग हैं, पर ‘हूँ’ सबमें एक है। ‘मैं’ तो बदला है, पर ‘हूँ’ नहीं बदला। वह ‘मैं’ बाप के सामने बेटा हो जाता, बेटे के सामने बाप हो जाता है अर्थात् वह जिसके सामने जाता है, वैसा ही हो जाता है। अगर उससे पूछें कि ‘तू कौन है’ तो उसको खुद का पता नहीं है ! यदि ‘मैं’ की खोज करें तो ‘मैं’ मिलेगा ही नहीं, प्रत्युत सत्ता मिलेगी। कारण कि वास्तव में सत्ता ‘है’ की ही है, ‘मैं’ की सत्ता है ही नहीं।
बेटे की अपेक्षा बाप है, बापकी अपेक्षा बेटा है—इस प्रकार बेटा, बाप, पोता, दादा आदि नाम अपेक्षासे (सापेक्ष) हैं; अतः ये स्वयं के नाम नहीं हैं। स्वयं का नाम तो निरपेक्ष ‘है’ है। वह ‘है’ ‘मैं’ को जाननेवाला है। ‘मैं’ जाननेवाला नहीं है और जो जाननेवाला है, वह ‘मैं’ नहीं है। ‘मैं’ ज्ञेय (जानने में आनेवाला) है और ‘है’ ज्ञाता (जाननेवाला) है। ‘मैं’ एकदेशीय है और उसको जानने वाला ‘है’ सर्वदेशीय है। ‘मैं’ से सम्बन्ध मानें या न मानें, ‘मैं’ की सत्ता नहीं है। सत्ता ‘है’ की ही है। परिवर्तन ‘मैं’ में होता है, ‘है’ में नहीं। ‘हूँ’ भी वास्तव में ‘है’ का ही अंश है। ‘मैं’ पनको पकड़ने से ही वह अंश है। अगर मैं-पन को न पकड़ें तो वह अंश (‘हूँ’) नहीं है, प्रत्युत ‘है’ (सत्ता मात्र है) ‘मैं’ अहंता और ‘मेरा बाप, मेरा बेटा’ आदि ममता है। अहंता-ममतासे रहित होते ही मुक्ति है—
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति।।
(गीता 2/71)
यही ‘ब्राह्मी स्थिति’ है। इस ब्राह्मी स्थितिको
प्राप्त
होनेपर अर्थात् ‘है’ में स्थिति का अनुभव होने पर
शरीर का कोई
मालिक नहीं रहता अर्थात् शरीर को मैं—मेरा कहनेवाला कोई नहीं
रहता।
मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, चूना है, पत्थर है—इस प्रकार वस्तुओं में तो फर्क है, पर ‘है’ में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ—इस प्रकार मनुष्य आदि योनियाँ तो बदली हैं, पर स्वयं नहीं बदला है। अनेक शरीरों में, अनेक अवस्थाओं में चिन्मय सत्ता एक है। बालक, जवान और वृद्ध—ये तीनों अलग-अलग हैं, पर तीनों अवस्थाओं में सत्ता एक है। कुमारी, विवाहिता और विधवा—ये तीनों अलग-अलग हैं, पर इन तीनोंमे सत्ता एक है। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा और समाधि—ये पाँचों अवस्थाएं अलग-अलग हैं, पर इन पाँचों में सत्ता एक है। अवस्थाएँ बदलती हैं, पर उनको जाननेवाला नहीं बदलता। ऐसे ही मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, और निरुद्ध—इन पाँचों वृत्तियों में फर्क पड़ता है, पर इनको जाननेवाले में कोई फर्क नहीं पड़ता।
--------------------------------------------------
मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, चूना है, पत्थर है—इस प्रकार वस्तुओं में तो फर्क है, पर ‘है’ में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ—इस प्रकार मनुष्य आदि योनियाँ तो बदली हैं, पर स्वयं नहीं बदला है। अनेक शरीरों में, अनेक अवस्थाओं में चिन्मय सत्ता एक है। बालक, जवान और वृद्ध—ये तीनों अलग-अलग हैं, पर तीनों अवस्थाओं में सत्ता एक है। कुमारी, विवाहिता और विधवा—ये तीनों अलग-अलग हैं, पर इन तीनोंमे सत्ता एक है। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा और समाधि—ये पाँचों अवस्थाएं अलग-अलग हैं, पर इन पाँचों में सत्ता एक है। अवस्थाएँ बदलती हैं, पर उनको जाननेवाला नहीं बदलता। ऐसे ही मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, और निरुद्ध—इन पाँचों वृत्तियों में फर्क पड़ता है, पर इनको जाननेवाले में कोई फर्क नहीं पड़ता।
--------------------------------------------------
एषा ब्राह्मी स्थितिः
पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।।
(गीता) 2/72)
‘हे पार्थ ! यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई
सम्मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अन्तकाल में भी स्थित हो जाय तो
निर्वाण (शान्त) ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।’
यदि जाननेवाला भी बदल जाय तो इन पाँचों की गणना कौन करेगा ? एक मार्मिक बात है कि सबके परिवर्तन का ज्ञान होता है, पर स्वयंके परिवर्तन का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। सबका इदंता से भान होता है, पर अपने स्वरूप का इदंता से भान कभी किसी को नहीं होता सबके अभाव का ज्ञान होता है, पर अपने अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। तात्पर्य है कि ‘है’ (सत्तामात्र) में हमारी स्थित स्वतः है करनी नहीं है। भूल यह होती है कि हम ‘संसार है’—इस प्रकार ‘नहीं’ में ‘है’ का आरोप कर लेते हैं। ‘नहीं’ में ‘है’ का आरोप करने से ही ‘नहीं’ (संसार) की सत्ता दीखती है और ‘है’ की तरफ दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में ‘है में संसार’—इस प्रकार ‘नहीं’ में ‘है’ का अनुभव करना चाहिये। ‘नहीं’ में ‘है’ का अनुभव करने से ‘नहीं’ नहीं रहेगा और ‘है’ रह जायगा।
भगवान् कहते हैं।
यदि जाननेवाला भी बदल जाय तो इन पाँचों की गणना कौन करेगा ? एक मार्मिक बात है कि सबके परिवर्तन का ज्ञान होता है, पर स्वयंके परिवर्तन का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। सबका इदंता से भान होता है, पर अपने स्वरूप का इदंता से भान कभी किसी को नहीं होता सबके अभाव का ज्ञान होता है, पर अपने अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। तात्पर्य है कि ‘है’ (सत्तामात्र) में हमारी स्थित स्वतः है करनी नहीं है। भूल यह होती है कि हम ‘संसार है’—इस प्रकार ‘नहीं’ में ‘है’ का आरोप कर लेते हैं। ‘नहीं’ में ‘है’ का आरोप करने से ही ‘नहीं’ (संसार) की सत्ता दीखती है और ‘है’ की तरफ दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में ‘है में संसार’—इस प्रकार ‘नहीं’ में ‘है’ का अनुभव करना चाहिये। ‘नहीं’ में ‘है’ का अनुभव करने से ‘नहीं’ नहीं रहेगा और ‘है’ रह जायगा।
भगवान् कहते हैं।
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।
(गीता 2। 16)
‘असत् की सत्ता विद्यमान नहीं है अर्थात् असत्का अभाव ही
विद्यमान
है और सत् का अभाव विद्यमान नहीं है अर्थात् सत् का भाव ही विद्यमान
है।’
एक ही देश काल वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि में अपनी जो परिच्छिन्न सत्ता दीखती है, वह अहम् (व्यक्तित्व, एकदेशीयता) को लेकर ही दीखती है। जबतक अहम रहता है, तभी तक मनुष्य अपने को एक देश, काल आदि में देखता है। अहम् के मिटने पर एक देश, काल आदि में परिच्छिन सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत अपरिच्छिन्न सत्तामात्र रहती है।
वास्तव में अहम है नहीं, प्रत्युत केवल उसकी मान्यता है। सांसारिक पदार्थों की जैसी सत्ता प्रतीत होती है, वैसी सत्ता भी अहम् की नहीं है। सांसारिक पदार्थ तो उत्पत्ति-विनाशवाले हैं, पर अहम् उत्पत्ति-विनाशवाला भी नहीं है। इसलिये तत्त्वबोध होने पर शरीरादि पदार्थ तो रहते हैं, पर अहम् मिट जाता है।
अतः तत्त्वबोध होने पर ज्ञानी नहीं रहता, प्रत्युत ज्ञानमात्र रहता है। इसलिये आजतक कोई ज्ञानी हुआ नहीं, ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी होगा नहीं और ज्ञानी होना सम्भव ही नहीं। अहम् ज्ञानी में होता है, ज्ञान में नहीं। अतः ज्ञानी नहीं है, प्रत्युत ज्ञानमात्र है, सत्तामात्र है। उस ज्ञानका कोई ज्ञाता नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, मालिक नहीं है। कारण कि वह ज्ञान स्वयंप्रकाश है, अतः स्वयं से ही स्वयं का ज्ञान होता है। वास्तव में ज्ञान होता नहीं है, प्रत्युत अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटाने को ही तत्त्वज्ञान का होना कह देते हैं।
एक ही देश काल वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि में अपनी जो परिच्छिन्न सत्ता दीखती है, वह अहम् (व्यक्तित्व, एकदेशीयता) को लेकर ही दीखती है। जबतक अहम रहता है, तभी तक मनुष्य अपने को एक देश, काल आदि में देखता है। अहम् के मिटने पर एक देश, काल आदि में परिच्छिन सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत अपरिच्छिन्न सत्तामात्र रहती है।
वास्तव में अहम है नहीं, प्रत्युत केवल उसकी मान्यता है। सांसारिक पदार्थों की जैसी सत्ता प्रतीत होती है, वैसी सत्ता भी अहम् की नहीं है। सांसारिक पदार्थ तो उत्पत्ति-विनाशवाले हैं, पर अहम् उत्पत्ति-विनाशवाला भी नहीं है। इसलिये तत्त्वबोध होने पर शरीरादि पदार्थ तो रहते हैं, पर अहम् मिट जाता है।
अतः तत्त्वबोध होने पर ज्ञानी नहीं रहता, प्रत्युत ज्ञानमात्र रहता है। इसलिये आजतक कोई ज्ञानी हुआ नहीं, ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी होगा नहीं और ज्ञानी होना सम्भव ही नहीं। अहम् ज्ञानी में होता है, ज्ञान में नहीं। अतः ज्ञानी नहीं है, प्रत्युत ज्ञानमात्र है, सत्तामात्र है। उस ज्ञानका कोई ज्ञाता नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, मालिक नहीं है। कारण कि वह ज्ञान स्वयंप्रकाश है, अतः स्वयं से ही स्वयं का ज्ञान होता है। वास्तव में ज्ञान होता नहीं है, प्रत्युत अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटाने को ही तत्त्वज्ञान का होना कह देते हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book